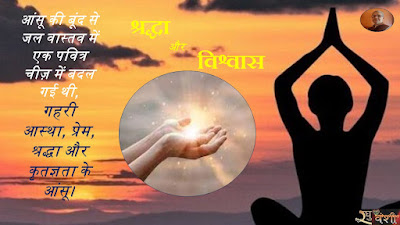आश्रम में आये अभी कुछ ही दिन हुए थे। लेकिन धीरे-धीरे पूरा शरीर विशेष कर दोनों पैर और कमर साथ नहीं दे रहे थे, पूरे बदन में दिन भर दर्द रहता था। चलना-फिरना, उठना-बैठना दूभर हो रखा था। किसी भी कार्य में एकाग्रता नहीं हो रही थी। पीड़ा के कारण आत्म-विश्वास की भी कमी हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या करूँ? केवल बिस्तर पर पड़े रहने से ही आराम मिल रहा था। आश्रम का कोई भी कार्य दिया जा रहा था तो बिना सोचे और लज्जा का अनुभाव किये तुरंत मना कर रहा था। क्या करता शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से लाचार था। कमरे में पड़े-पड़े निबंधों को जाँचने का काम, कुछ नया लिखने- पढ़ने का काम भी नहीं कर पा रहा था। आश्रम में इस प्रकार पड़े रहने में शर्म भी महसूस हो रही थी। अंग-प्रत्यंग ही नहीं बल्कि आवाज में भी पीड़ा की झलक थी, चेहरे पर तो सब लिखा हुआ ही था। ज्योति दीदी ने भाँप लिया था शायद इसीलिये कई बार पूछ चुकी थीं, ‘भैया, आप ठीक तो हैं न।’ क्या कहता, झिझक में सही बता भी नहीं पा रहा था। ‘हाँ, हाँ ठीक ही हूँ।’ यही कहता रहा।
हर दिन की तरह आज भी मुंह-अंधेरे
नींद खुल गई। आज तो बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। आज सुबह की सैर पर नहीं जा
सकूँगा, यह निश्चय कर मुंह ढक कर वापस सो गया।
लेकिन तभी चेतना उठ खड़ी हुई। कल की कक्षा में क्या पढ़ा-सुना?
आवाज आई, उठ, आज अभी इसे आजमा कर देख
ले कैसा रहता है।
कौन-सी कक्षा और क्या पढ़ाई? संकल्प, अभीप्सा और अध्यवसाय। श्री
अरविंद और श्री माँ की कृतियों से चयनित अंशों पर आधारित पुस्तक ‘Living
Within’ का हिन्दी रूपान्तरण ‘आंतरिक रूप से
जीना’ हमारी मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और प्रगति के लिये सहायक
पुस्तक है। इस पुस्तक की चल रही कक्षा में कल का यही विषय था – संकल्प, सच्चाई या अभीप्सा और अध्यवसाय से हम कैसे रूपांतरित हो सकते हैं, कैसे? कल इस अनुच्छेद को हमने पढ़ा था –
“पहला पग है : संकल्प। दूसरा है सच्चाई और अभीप्सा। परन्तु
संकल्प और अभीप्सा लगभग एक ही चीज है, एक-दूसरे के अनुगामी हैं। फिर है, अध्यवसाय। हां,
किसी भी प्रक्रिया में अध्यवसाय आवश्यक है, और यह प्रक्रिया क्या है?... प्रथम, निरीक्षण और विवेक करने की योग्यता
अवश्य होनी चाहिये,
अपने अन्दर प्राण को खोज निकालने की योग्यता अवश्य होनी
चाहिये,
नहीं तो तुम्हारे लिये यह कहना कठिन हो जायेगा कि, "यह प्राण से आता है, या मन से आता है, यह शरीर से आता है।" प्रत्येक चीज तुम्हें मिली-जुली और अस्पष्ट प्रतीत
होगी। बहुत दीर्घकालिक निरीक्षण के बाद,
तुम विभिन्न भागों के बीच विभेद करने तथा क्रिया का मूल समझने में समर्थ हो सकोगे।
इसमें अत्यंत लंबे समय की आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य
तेज भी जा सकता है। ( पृ 92)
इस पर चर्चा करते हुए ज्योति
दीदी ने बताया कि मन केवल चंचल ही नहीं बहुत हठी भी है और समझदार भी, एक छोटे बच्चे की तरह। अपनी जिद नहीं छोड़ता और अपना कार्य
करवाने के सब गुर जानता है। उसे डांट कर या मार कर नहीं समझाया जा सकता है। जैसे
छोटे बच्चे को समझा-बुझा कर ही मनाया जा सकता है वैसे ही उसे समझाना होता है।
इसे ही
आजमाने का निश्चय किया, और मैंने एक छोटे बच्चे की तरह उसे समझाना
शुरू किया – चल उठ खड़ा हो, नीचे चल।
‘ऊँह, नहीं जाना,
बहुत दर्द है, ठंड भी है और अभी तो दिन भी नहीं हुआ है।’ उसने तीन-तीन कारण गिना दिये। लगा स्थिति जटिल है,
लेकिन आज मैं भी हारने के लिये तैयार नहीं था। धीरे-धीरे प्यार से समझाना शुरू
किया, ‘दर्द मिटाना है न, बिस्तर में पड़े रहने से दर्द कम नहीं ज्यादा हो जायेगा। तब चल-फिर और बैठ
भी नहीं पाओगे। उठ गरम जैकेट पहन ले ठंड नहीं लगेगी और तैयार होते-होते दिन भी निकल
आयेगा।’
‘नहीं, आज नहीं कल’, उसने बहाना बनाया।
‘आज नहीं जाओगे तो कल भी नहीं जाने सकोगे।
दर्द बढ़ जायेगा, थोड़ा चलोगे तो दर्द कम हो जायेगा।’
लेकिन, शरीर किसी भी तरह उठने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन आज मैं
भी जिद पर था। तरह-तरह से समझाता रहा, अंत में उसके पसंदीदा रेस्टुरेंट
में ले जाने का प्रलोभन दिया, तब शरीर कुछ हिला, ‘तुम बहुत लंबा घुमाते हो,
उतना नहीं घूम सकूँगा। इतने चक्कर नहीं लगाऊँगा।’
‘अच्छा ठीक है आधा चक्कर ही लगाएंगे।’
‘पक्का?’
‘हाँ पक्का’, मैंने वचन
दे दिया।
आखिर शरीर मान ही गया। और हम घूमने उतर गये। लेकिन आधी दूरी
पूरी हुई ही नहीं थी कि वह फिर से उठ खड़ा हुआ,
‘आधा हो गया, अब वापस चलो।’
‘नहीं’, मैंने अंगुली
से दिखाया, ‘वहाँ पहुंचने पर आधा होगा
न।’
‘चलो, अब लौटो, आधा हो गया।’ कुछ ही देर बाद उसने फिर से कहा।
‘हमलोग गोल-गोल घूम रहे हैं, आधी दूर आ गये, अब वापस जाएँ या आगे चलें बात तो एक
ही है, तब आगे ही चलें’, मैंने समझाया।
उसे बात पसंद तो नहीं आई, षड्यंत्र की गंध आई लेकिन मान
गया। पूरा होने पर मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, ‘ये क्या! हो गया अब आगे नहीं।’
‘अरे घूमने नहीं जा रहे हैं सामने श्री
अरविंद को प्रणाम करके लौटेंगे।’ और इस प्रकार समाधि, फूल, तुलसी, मोर और सूर्योदय
का लालच देकर मैंने दो चक्कर लगवा ही लिये।
मन बहुत
प्रसन्न था। अच्छा भी लग रहा था – शरीर और मन दोनों को। कल की पढ़ाई आज ही काम आ
गई। संकल्प लिया मुझे आज ही ठीक होना है,
सोच-विचार कर सुबह-सुबह दो-तीन उपचार किया और बात बन गई। सारी पीड़ा रफू-चक्कर हो
चुकी थी और पूर्ण स्वस्थ्य महसूस करने लगा। दोपहर में भोजन-कक्ष में दीदी से
मुलाक़ात हुई, मैंने चहकते हुए पूछा, ‘दीदी, आज कैसा लग रहा हूँ।’
‘अभी तो आप ठीक लग रहे हैं भैया।’
‘अपने ही तो ठीक किया है’
‘…….’ दीदी मुझे देखने लगी, मैंने पूरा वाकिया सुनाया।
‘मैंने नहीं, माँ ने
ठीक किया है।’
‘हाँ, लेकिन वे आईं तो
आपके ही रूप में न।’
मेरा रूपान्तरण हो चुका था।
पढ़ने से, सुनने से, सोचने से कुछ नहीं होता।
संकल्प लेकर पूरी सच्चाई और अभीप्सा से अध्यवसाय करने से ही फल की प्राप्ति होती
है।
यह प्रत्यक्ष अनुभव था।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
लाइक करें, सबस्क्राइब करें, परिचितों
से
शेयर करें।
अपने सुझाव ऑन
लाइन दें।
यू ट्यूब पर सुनें
: à